यूनिफार्म सिविल कोड पर बड़ी बहस शुरू, क्या पड़ेगा धार्मिक-मज़हबी मान्यताओं पर असर ?

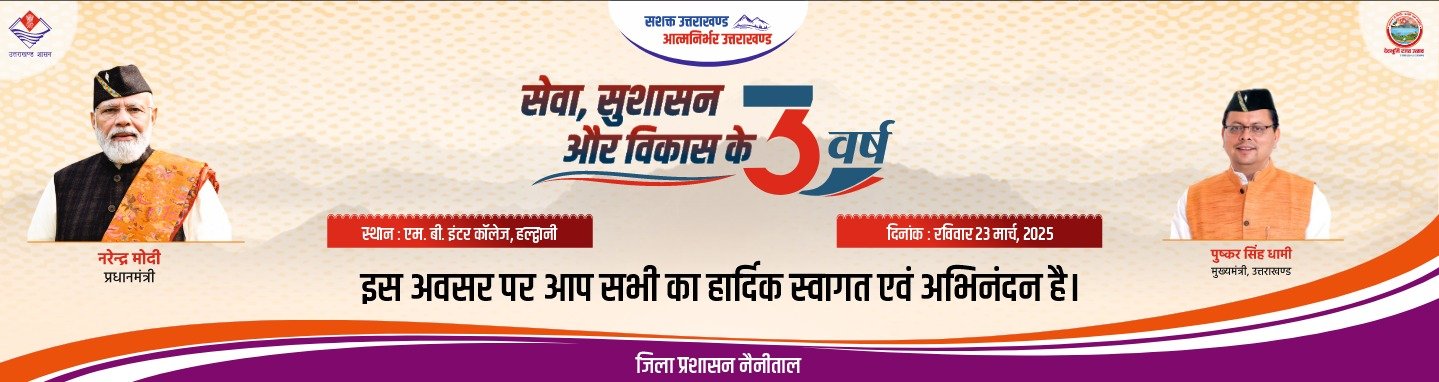
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने की बातें होने लगी हैं. सुप्रीम कोर्ट भी कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत की बात कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भारत में अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया. जबकि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में नीति निदेशक तत्व के तहत उम्मीद जताई थी कि भविष्य में ऐसा किया जाएगा. इस लेख में हम इससे जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर बारीक चर्चा करेंगे.
क्या है समान नागरिक संहिता
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम. दूसरे शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता. इस वक्त हमारे देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग नियमों को मानने की छूट है. जैसे- किसी समुदाय में बच्चा गोद लेने पर रोक है. किसी समुदाय में पुरुषों को कई शादी करने की इजाज़त है. कहीं-कहीं विवाहित महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा न देने का नियम है. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं होंगे.
धार्मिक मान्यताओं पर फर्क नहीं
यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब कतई नहीं है कि इसकी वजह से विवाह मौलवी या पंडित नहीं करवाएंगे. ये परंपराएं बदस्तूर बनी रहेंगी. नागरिकों के खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर इसका कोई असर नहीं होगा.
संविधान में भी है जिक्र
संविधान बनाते वक्त समान नागरिक संहिता पर काफी चर्चा हुई. लेकिन तब की परिस्थितियों में इसे लागू न करना ही बेहतर समझा गया. इसे अनुच्छेद 44 में नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी में जगह दी गई. नीति निदेशक तत्व संविधान का वो हिस्सा हैं जिनके आधार पर काम करने की सरकार से उम्मीद की जाती है.
1954-55 में भारी विरोध के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू हिंदू कोड बिल लाए. इसके आधार पर हिन्दू विवाह कानून और उत्तराधिकार कानून बने. मतलब हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे नियम संसद ने तय कर दिए. मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों को अपने-अपने धार्मिक कानून यानी पर्सनल लॉ के आधार पर चलने की छूट दी गई. ऐसी छूट नगा समेत कई आदिवासी समुदायों को भी हासिल है. वो अपनी परंपरा के हिसाब से चलते हैं.
लॉ कमीशन ने सीधे लागू करने से मना किया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लॉ कमीशन को मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था. पिछले साल 31 अगस्त को लॉ कमीशन ने यूनिफार्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ में सुधार पर सुझाव दिए. अलग-अलग लोगों से विस्तृत चर्चा और कानूनी, सामाजिक स्थितियों की समीक्षा के आधार पर लॉ कमीशन ने कहा, “अभी समान नागरिक संहिता लाना मुमकिन नहीं है. इसकी बजाय मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार किया जाए. मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता में संतुलन बनाया जाए. पारिवारिक मसलों से जुड़े पर्सनल लॉ को संसद कोडिफाई करने (लिखित रूप देने) पर विचार करे. सभी समुदायों में समानता लाने से पहले एक समुदाय के भीतर स्त्री-पुरुष के अधिकारों में समानता लाने की कोशिश हो.
कई याचिकाएं हैं लंबित
यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करने वाली कई याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित हैं. यह याचिकाएं अश्विनी उपाध्याय, फ़िरोज़ बख्त अहमद, अंबर ज़ैदी, निगहत अब्बास और दानिश इकबाल जैसे कई लोगों की की हैं. इन सभी याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह मामला अपने पास ट्रांसफर ले ले. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्म की महिलाओं के लिए एक समान गुज़ारा भत्ता, शादी की एक समान उम्र की मांग, गोद लेने के लिए एक जैसा कानून, मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति जैसे मसलों पर याचिकाएं लंबित हैं. यह सभी विषय नागरिकों के लिए एक जैसे सिविल कानून की ही मांग करते हैं.
क्या राज्यों का इसे लागू करना व्यवहारिक होगा?
विवाह, तलाक, वसीयत जैसे तमाम विषयों पर केंद्रीय कानून हैं. हिंदुओं के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार कानून जैसे एक्ट हैं, तो मुसलमानों के सिविल मामले एप्लिकेशन ऑफ शरीयत एक्ट, 1937 से संचालित होते हैं. केंद्रीय कानूनों के रहते राज्यों का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत प्रभावी नहीं होगा. अगर राज्य ऐसा करते हैं तो उसकी वैधता को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.


लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com




 हाईवे हादसा : हमेशा के लिए थम गई दो धड़कनें, खाई से निकाले गए पति-पत्नी के शव..
हाईवे हादसा : हमेशा के लिए थम गई दो धड़कनें, खाई से निकाले गए पति-पत्नी के शव..  हल्द्वानी – खूनी सड़क हादसे का CCTV फुटेज सामने आया,,जांच शुरू..
हल्द्वानी – खूनी सड़क हादसे का CCTV फुटेज सामने आया,,जांच शुरू..  हल्द्वानी में कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कर का पत्रकारों ने किया स्वागत..
हल्द्वानी में कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कर का पत्रकारों ने किया स्वागत..  Haldwani : कुमाऊं प्रीमियर लीग में नैनीताल बना चैंपियन_ पिथौरागढ़ को हराया..
Haldwani : कुमाऊं प्रीमियर लीग में नैनीताल बना चैंपियन_ पिथौरागढ़ को हराया..  Haldwani में खुदी सड़क और ट्रक की टक्कर से बुजुर्ग की बेहद दर्दनाक मौत..
Haldwani में खुदी सड़क और ट्रक की टक्कर से बुजुर्ग की बेहद दर्दनाक मौत..